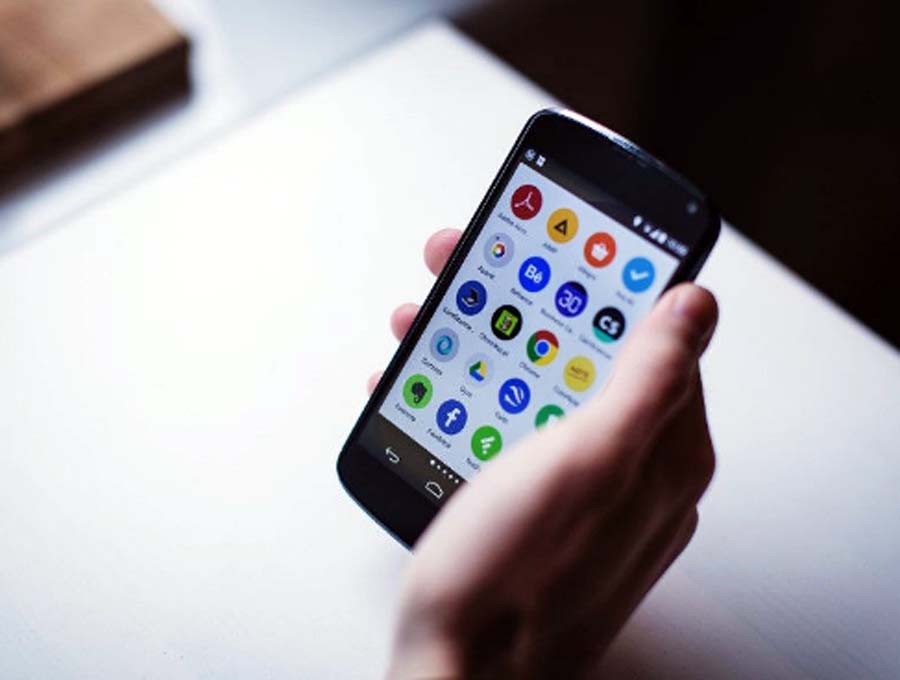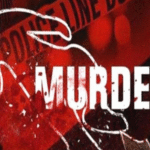किसी भी राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक वहां के नौनिहालों पर आश्रित होता है। ऐसे में राष्ट्र के बेहतर आगामी कल के लिए नौनिहालों को वर्तमान में बेहतर तालीम मिलनी चाहिए। बच्चों के सामाजिक विकास और चरित्र निर्माण में स्कूली शिक्षा का अहम योगदान है। ऐसे में जब स्कूल खुलने को हैं, या खुल चुके हैं। बच्चों को सरकारी स्कूल तक लाने की पुरजोर कोशिश चल रही। जिससे सरकारी तंत्र पीठ थपथपा सकें, कि उसने अपना कार्य निष्पादित कर दिया। लेकिन ऐसे में इक्कीसवीं सदी के भारत में, जब वह विश्वगुरु बनने को लालायित दिख रहा। तो कल्पना कीजिए। देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पर संवैधानिक देश की बिडंबना है। डिजिटल होते भारत की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था ही सुविधाओं के अभाव में चरमरा चुकी है।
यहां हम एक दृश्य का नजारा पेश करते हैं। जर्जर भवन, कहीं छत ही नहीं, छत है भी तो वह टपकती हुई, ऊबड़-खाबड़ रास्ते, बिजली का अभाव उस दौर में जब राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी पीठ थपथपा रहें कि हर घर और जगह को रोशनी से जगमग कर दिया गया है। कल्पना कीजिए यह दृश्य किस जगह का होगा। कल्पनाओं में ज्यादा देर गोते लगाने की जरूरत नहीं। यह किसी सुदूर अंचल के गांव- गरीब के घर का चित्रण नहीं। यह तो विद्या के मंदिर का चित्रण है। जहां देश का भावी भविष्य तैयार किया जा रहा।
गौरतलब हो, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा को लेकर नियम-कानून बनाने का अधिकार रखती, लेकिन बच्चों को लेकर वह सोचती कहाँ? उन्हें तो वंदे मातरम, और हिन्दू-मुस्लिम करने से इतर फुर्सत कहाँ? अरे भाई कोई इन संवैधानिक तंत्र को सुशोभित करने वाले रणबाकुरों को यह तो बता दें, जब बच्चे शिक्षित होंगे। तभी तो वे आगे चलकर बेहतर राष्ट्र के निर्माण के सहभागी बनेंगे। ऐसे में नौनिहालों के लिए बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का इंतजाम करने पर ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य देखिए देश के भविष्य का। देश में शिक्षा नीति को लेकर आजादी के बाद से कई आयोग बन चुके हैं। मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। जिसमें 1992 में संशोधन हुआ। वर्तमान में एक नई शिक्षा नीति पर बहस चल रही। देश त्रिभाषा फार्मूले पर अटका हुआ है।
ऐसी स्थिति में आकर कई सवाल उपजते हैं। सवाल यह देश ने आजादी के बाद से कई शिक्षा नीतियां देखी हैं, तो क्या आज बच्चों के लिए स्कूल की डगर आसान है? शिक्षा नीति पर बहस तो होती है, लेकिन उन पर अमल क्यों शत-प्रतिशत नहीं हो पाता? शिक्षा के अधिकार को आए एक दशक हो गए, उसके द्वारा अपने लक्ष्य पूरे करने में हाथ-पांव क्यों फूल रहें? क्या सरकारी तंत्र चाहे केंद्र का हो या राज्य का। वह इस कदर कुम्भकर्णी नींद में है। जिसे देश के पालय की फिक्र नहीं?
ये सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि तत्कालीन दौर में सरकारी स्कूलों के हाल समूचे देश मे किस तरह हैं। वह किसी से छिपे नहीं हैं। तमाम आयोगों के गठन, संवैधानिक अधिकारों के अलावा शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे नौनिहालों तक नहीं पहुँच पाई है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल मोटी फीस के बल पर फलते-फूलते जा रहे। मानते हैं, प्राइवेट स्कूल की शिक्षा निसंदेह सरकारी स्कूलों से बेहतर होती, लेकिन भारी भरकम फीस का इंतजाम उस देश में सभी कर लें, जहां पर गरीबी की परिधि 27 रुपए में नापी जाती यह सम्भव तो नहीं ! ऐसे में क्या हुकूमत में बैठे सियासतदानों का यह कर्तव्य नहीं, कि वे हर बच्चे तक निशुल्क और बेहतर शिक्षा पहुचाएं। ज्ञान के मंदिर की हालत बद्दतर जिस हिसाब से पूरे देश में है। ऐसे में तो कभी कभार ऐसा मालूम पड़ता है, कि बच्चों के सामान्य ज्ञान के लिए शिक्षामंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम बदल जाने से विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। जब शिक्षा की हालत और अगर स्कूलों की दशा- दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है।
अगर स्कूली शिक्षा की इतनी ही विकट नहीं। शिक्षा मंत्रालय के एक आँकड़े के मुताबिक देश के स्कूलों में दाखिला लेने वाले 100 बच्चों में से 70 बच्चें ही बारहवीं तक पढ़ाई कर पाते हैं। झारखंड में तो यह आंकड़ा 30 का ही है। वहीं देश के 92 हजार 275 स्कूल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे हैं, जहां एक शिक्षक ही भगीरथ की भूमिका में है। ऐसे में बात ये कि आज का शिक्षक भगीरथ जैसा दृढ़निश्चयी तो होगा नहीं। फिर देश की नींव भावी भविष्य के लिए खड़ी की जा रही। समझ से बाहर है। कहीं शिक्षा की अनदेखी हमारे रहनुमा इसलिए तो नहीं कर देते, क्योंकि वे अनपढ़ होने पर भी लोकतंत्र के मंदिर के संरक्षक बन जाते हैं? विभिन्न रिपोर्ट्स और आंकड़े कहते हैं, कि 25 फीसदी युवा अपनी मातृभाषा में लिखे को धाराप्रवाह नहीं पढ़ पाते। ऐसे में उन मातृभाषा के ठेकेदारों को भी इस आंकड़े से सीख लेनी चाहिए, जो हिंदी का नाम आते ही छाती पीटने लगते है कि हिंदी उन पर थोपी जा रहीं। तो हिंदी का विरोध ही करना है, तो करें लेकिन पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो आवाज को बुलंद करें। अब बात आधी आबादी की करें, तो 18 वर्ष से कम उम्र की 32 फीसदी लड़कियां स्कूली शिक्षा के दायरे में आती ही नहीं।
वह भी उस दौर में जब शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के नौनिहालों को मुफ़्त शिक्षा और आधी आबादी को उसका हक देने की बात जोर-शोर से हवा में गूंजता दीप्तिमान होता है। इसके अलावा जिस दौर में 14 से 18 वर्ष के 42 फीसदी युवा जीवनयापन करने के लिए काम करते हैं, दूसरी और 77 फीसदी लड़कों और 89 फीसदी लड़कियों को गृह कार्यों में हिस्सेदारी लेनी पड़ती है। तो अब इस नियम की सख्त जरूरत है, कि 6 से 18 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा को मुफ़्त किया जाए। जिसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। यहां एक बात यह भी शिक्षा को मुफ़्त कर देना ही समाधान नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद भी सिर्फ मध्यप्रदेश सूबे में पिछले 5 वर्षो में हर वर्ष पहली से आठवीं तक के लगभग 3 से 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की ओर पलायन कर गए हैं। ऐसे में शिक्षा पर खर्च के बजट को 6 फीसदी करना होगा। जिसकी मांग वर्षों से हो रही। वहीं केरल और दिल्ली सरकार की पहल का अनुसरण भी हमारे देश के बाकी राज्य करते हैं।
तो हमें विदेशों से सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके लिए बाकी राज्यों में वैसी नीति और नियत पैदा करनी होगी। इन सब बातों के अलावा अगर नई शिक्षा नीति को देश और प्रदेश के लिए तैयार करने के साथ हमारी नीतियों में अतीत की गुरुकुल व्यवस्था से कुछ सीख ली जाती है, और शिक्षकों की कमी को पूरे देश में खत्म किया जाता है। बेहतर नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन होता है। तभी सरकारी स्कूल की स्थिति सुधर सकती है। ऐसे में तमाम कदम उठाने के साथ अगर एक ऐसा नियम बनाया जाए, जिसके तहत सरकारी तंत्र में बैठे लोग और प्रशासनिक अधिकारी के पाल्य सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। फिर इसी बहाने गरीबों और वंचितों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण तालीम मिल सकती है। महेश तिवारी
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करे।