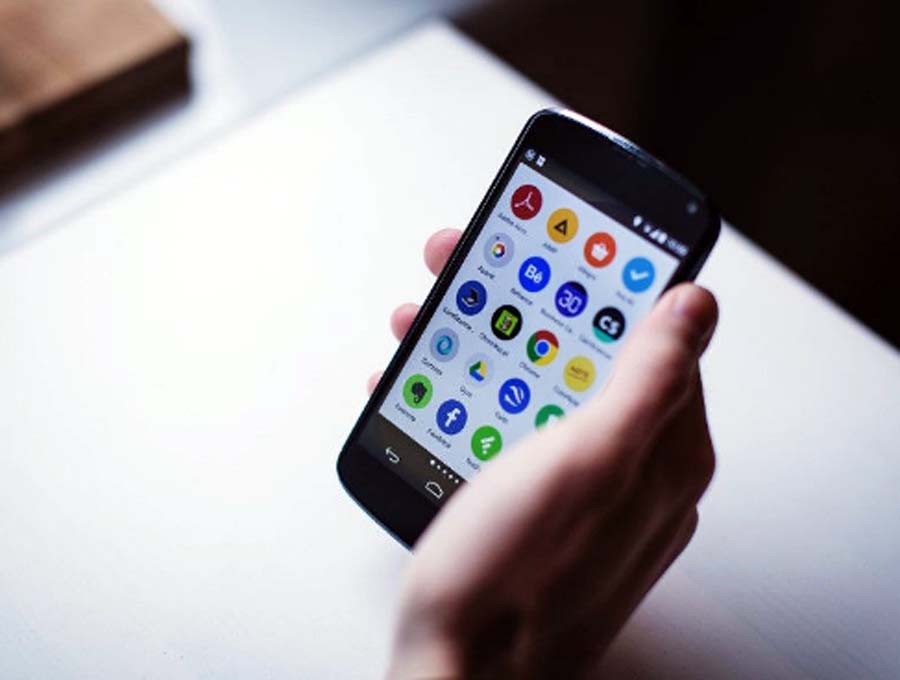पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश भर में धान की पराली कहीं भी नहीं जलाई जाती। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो अधिकांश धान हाथ से काटा जाता है और फिर हाथ से ही झाड़ कर निकाला जाता है। हाथ से काटने और झाड़ने में एक तो कोई प्रदूषण नहीं होता, डीजल का खर्चा बचता है और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को खूब रोजगार भी मिलता है। वास्तव में, कृषि में मानव श्रम की भागीदारी कम होने और कृषि मशीनरी के अधिक उपयोग से पराली की समस्या विकट हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के राज्यों में पराली जलाने के समाचार आने लगे हैं। हर वर्ष धान की कटाई के बाद ये समस्या मुंह बायें खड़ी हो जाती है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई वर्षों के प्रयासों के उपरांत भी इस समस्या का कोई समुचित समाधान नहीं हो पाया है। पराली जलाने वाले किसानों के अपने तर्क और समस्याएं हैं। तमाम तर्कों और उपायों के उपरांत, हर वर्ष दिल्ली-एनसीआर में पड़ोसी प्रदेशों से पराली के धुएं से उठती जहरीली हवाएं दमघोंटू वातावरण निर्मित कर देती हैं। ऐसे में अहम प्रश्न यह है कि अन्तत: इस विकट समस्या का निदान क्या है? वो कौन से उपाय है जिनकों अपनाकर इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है? वास्तव में, कृषि में मानव श्रम की भागीदारी कम होने और कृषि मशीनरी के अधिक उपयोग से पराली की समस्या विकट हुई है।
प्रदूषण का आंकलन करने वाली सरकारी संस्था ‘सफर’ के अध्ययन के अनुरूप बीते वर्ष दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी अधिकतम 46 प्रतिशत पर रही, जो दिवाली से पहले सामान्यत: 15 प्रतिशत से नीचे थी। जिसमें अन्य कारक मिलकर समस्या को और जटिल बना देते हैं। किसान स्वयं भी पराली जलाने के दुष्परिणाम जानते हैं पराली की समस्या का आखिर उचित हल क्या है और क्या इसे जलाने के लिए केवल किसान जिम्मेदार हैं? कृषि एक आर्थिक गतिविधि है। लाभ-हानि किसान के निर्णय को प्रभावित करते हैं। किसान स्वयं भी पराली जलाने के दुष्परिणाम जानते हैं और इनके प्रति सचेत हो रहे हैं।
वैज्ञानिक एवं कृषि विशेषज्ञों की चिंता का कारण यह है कि पराली जलाने की प्रक्रिया में कॉर्बनडाइआॅक्साइड व घातक प्रदूषण के कण अन्य गैसों के साथ हवा में घुल जाते हैं जो सेहत के लिये घातक साबित होते हैं। निश्चय ही जटिल होती समस्या हवा की गति, धूल व वातावरण की नमी मिलकर और जटिल हो जाती है। पिछले साल आईआईटी, कानपुर ने एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन के अनुरूप इन महीनों में दिल्ली के प्रदूषण में अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सा ही पराली जलाने के कारण होता है। राजधानी दिल्ली व एनसीआर का स्थानीय प्रदूषण भी अत्यधिक होता है।
पराली जलाने की समस्या से देश का सर्वोच्च न्यायालय भी चिंतित है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने कृषिभूमि में पराली जलाने के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र व निकटवर्ती राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली सरकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चेताया कि यदि समय रहते इस दिशा में कोई कार्रवाई न हुई तो स्थिति बिगड़ जाएगी। ऐसे समय में जब जब देश में कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, वायु प्रदूषण समस्या को और विकट बना सकता है। अवश्य ही यह कहा जा सकता है कि समस्त प्रयासों व दावों के बावजूद कृषि भूमि में पराली जलाने की समस्या नियंत्रण में नहीं आ रही है। पंजाब में किसानों की शिकायत है कि राज्य सरकार उन्हें अवशेष को न जलाने के प्रतिफल में क्षतिपूर्ति देने में असफल रही है।
वर्तमान परिस्थितियों में वे पराली के निस्तारण के लिये क्रय की जाने वाली मशीनरी हेतु ऋण भुगतान करने में भी सक्षम नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री का दावा है कि उन्होंने पराली प्रबंधन की लागत कम करने के लिये केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य किया है। पराली जलाने वाले प्रदेशों पंजाब और हरियाणा में एक तो मजदूरी महंगी है और दूसरे धान की कटाई के वक्त पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध भी नहीं हो पाते। दरअसल मनरेगा जैसी योजनाओं के चलते किसानों को सस्ते मजदूर नहीं मिलते। पंजाब और हरियाणा में पहले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मजदूर आया करते थे परन्तु अब स्थानीय स्तर पर अपने राज्यों में ही मनरेगा के माध्यम से मजदूरी मिलने के चलते कम संख्या में ही ये पलायन करते हैं। इस बार कोविड के कारण मजदूरों का पलायन भी बड़ी समस्या बनकर सामने आया है।
जमीनी सच्चाई यह भी है कि किसानों को अक्टूबर में खेत खाली करने की जल्दी भी रहती है क्योंकि उन्हें अपनी रबी की फसल आलू, मटर, सरसों, गेंहंू आदि की बुवाई के लिए भी खेत तैयार करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। मशीन से कटाई तेज भी होती है और ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती परन्तु इसमें डीजल के प्रयोग से प्रदूषण जरूर होता है। पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश भर में धान की पराली कहीं भी नहीं जलाई जाती। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो अधिकांश धान हाथ से काटा जाता है और फिर हाथ से ही झाड़ कर निकाला जाता है। हाथ से काटने और झाड़ने में एक तो कोई प्रदूषण नहीं होता, डीजल का खर्चा बचता है और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को खूब रोजगार भी मिलता है।
मशीन से कटाई के बाद पराली जलाने से केवल प्रदूषण ही नहीं होता बल्कि जमीन से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों और जमीन की उर्वरता का भी नुकसान होता है। इस कारण अगली फसल में और अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे देश पर खाद सब्सिडी का बोझ भी बढ़ता है और किसानों की लागत भी। धरती का तापमान भी बढ़ता है, जिसके बहुत से अन्य गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। आग में कृषि में सहायक केंचुए, अन्य सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। इससे भविष्य में फसलों की पैदावार बड़ी मात्रा में घट सकती है और देश में खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। पराली से बिजली बनाने या उसका कोई अन्य प्रयोग करने वाले सुझाव भी सीधे या परोक्ष रूप से प्रदूषण को ही बढ़ाते हैं। मशीनों से पराली प्रबंधन के लिए जो उपाय सुझाये गये हैं उनकी अपनी समस्यायें भी हैं।
सुझाव दिया जाता रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उन्हीं किसानों को मिले जो पराली का निस्तारण ठीक ढंग से करते हैं। ऐसे वक्त में जब दीवाली का त्योहार भी करीब है, समस्या के विभिन्न कोणों को लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। साथ ही किसानों को जागरूक करने की भी जरूरत है कि भले ही किसान को पराली जलाना आसान लगता हो, मगर वास्तव में यह खेत की उर्वरता को नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन समस्या यह भी है कि छोटे व मझोले किसान पराली निस्तारण के लिये महंगी मशीन खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इस दिशा में सब्सिडी बढ़ाने की भी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। निस्संदेह खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिये किसानों को जागरूक करने की भी जरूरत है। किसानों को दंडित किये जाने के बजाय उनकी समस्या के निस्तारण में राज्य तंत्र को सहयोग करना चािहए।
पराली जलाने की घटनाएं हर वर्ष होती हैं। विडंबना ही है कि पराली के कारगर विकल्प के लिये केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से समस्या विकट होने पर ही पहल की जाती है, जिससे समस्या का कारगर समाधान नहीं निकलता। कारण यह भी है कि साल के शेष महीनों में समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक सस्ता और सरल उपाय तलाशा है। उसने एक ऐसा घोल तैयार किया है, जिसका पराली पर छिड़काव करने से उसका डंठल गल जाता है और वह खाद में परिवर्तित हो जाता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाये गये किसान सुधार बिलों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच इस समस्या से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है।
-आशीष वशिष्ठ
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।